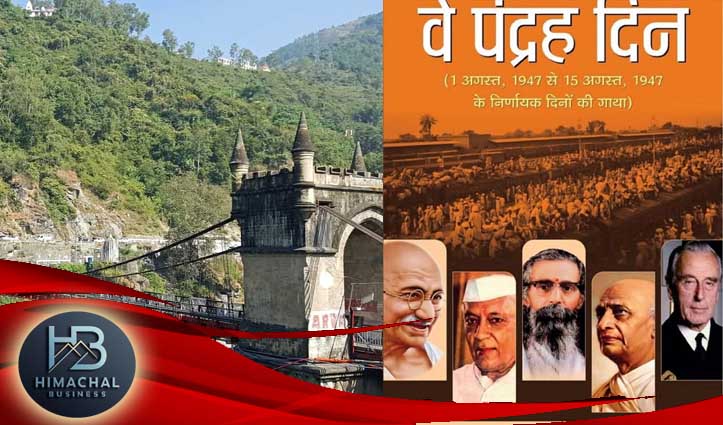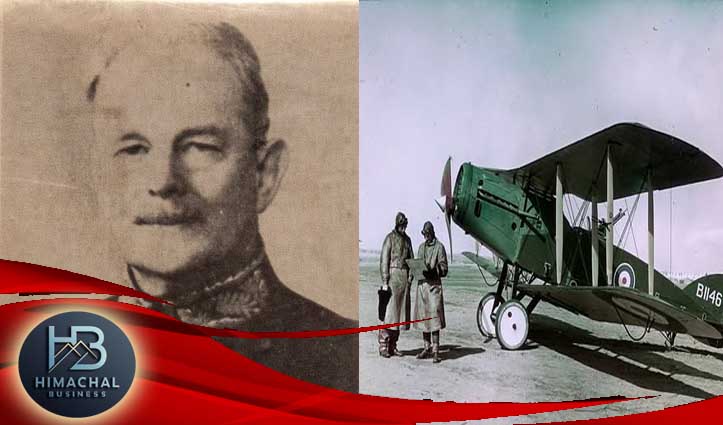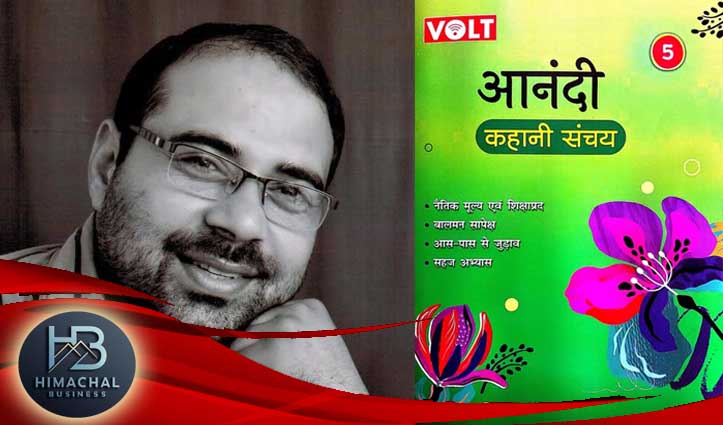देव सहारे लोक संस्कृति का संरक्षण

प्रो. सुंदर लोहिया/ स्तंभकार
इस उपभोक्तावादी युग में भी लोक संस्कृति को बचाने की गुहार लगाते रहते हैं। संस्कृति के प्रति उनकी अनुरक्ति के कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संस्कृति लोकरंजन का सशक्त और परखा हुआ माध्यम है, पर कुछ लोगों के लिए यह ऐसा उत्पाद है जिसकी रिपैकिंग करके बेचा जा सकता है।
कानफोडू संगीत के इस दौर में यदि कभी कोई लोकगीत सुनाई पड़ जाए, तो कुछ लोगों के पांव आज भी थम जाते हैं। लोक संस्कृति संरक्षण के नाम पर जो प्रयास हो रहे हैं, वे वास्तव में अपसंस्कृति के प्रसार में मददगार हैं।
सामूहिक रचनाएं होती हैं लोकगीत

लोकगीतों के नाम पर रिमिक्स के एलबम या किसी पहाड़ी कवि जो गायक भी है, उसके लिखे गीत लोकगीत के तौर पर प्रचारित किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें लोकगीत नहीं माना जा सकता। लोकगीत सामूहिक रचनाएं होती हैं। इनका कोई एक व्यक्ति रचनाकार नहीं होता है। समूह में इकट्ठे काम कर रहे लोग अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक उसमें योगदान करते आए हैं।
एक व्यक्ति भावावेश में लयबद्ध पंक्ति बोलता है, तो समूह का कोई दूसरा व्यक्ति उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ देता है। यदि बाद में जोड़ी गई पंक्ति किसी तरह से फिट न बैठे, तो तो उसे दोहराने वाले गायक नहीं मिलते और इसलिए उसे छोड़ कोई ओर लाइन जोड़ देता है ।
इसलिए लोकगीत की लय और शब्द बदलते रहते हैं, लेकिन उसका सामूहिक चरित्र बना रहता है, जो उसकी असल पहचान है। आज जब कृषि प्रौद्योगिकी इतनी विकसित हो चुकी है कि धान रोपने, गेहूं काटने जैसे सामूहिक कृषि कार्यों को अब एक कंबाइंड हार्वेस्टर के माध्यम से पूरा कर लिया जाता है, इसलिए कृषि से जुड़ी हुई सामूहिकता समाप्त हो गई है।
लोकगीतों के निर्माण की संभावना समाप्त
यही से लोक संस्कृति के विकास की संभावना कम से कम लोकगीतों के निर्माण को लेकर तो समाप्त ही हो चुकी है। अब उसे बचाने के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। इसे बचाया ही जा सकता है, दोहराया नहीं जा सकता।
यानी आज हम यह नहीं सोच सकते कि कुल्लवी नाटी भरमौर की घुरई, कांगड़ा का झमाकड़ा और मंडी की लुड्डी उसी रूप में चलती रहे या गोहर के शहनाई वादक चिरंजीलाल शनाई बजाता रहे। संस्कृति के संरक्षण के लिए सामाजिक परिस्थितियों को यथावत बनाए रखने की जरूरत होती है, क्योंकि संस्कृति सामाजिक- आर्थिक परिस्थितियों की उपज होती है।
परिस्थितियां बदलें तो लोक संस्कृति में परिवर्तन
अतः जब ये परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो संस्कृति में भी परिवर्तन उभर आते हैं, इसलिए यदि हम गोहर के चिरंजीलाल की शहनाई का रसास्वादन करना चाहते हैं, तो चिरंजीवाल की जीविका का जिम्मा भी तो उठाना पड़ेगा। उसे जिंदा रखने की जिम्मेदारी हम सरकार पर थोप कर पल्ला झाड़ लेते हैं और चिरंजीलाल को जिंदा रहने की लड़ाई खुद लड़ने के लिए विवश कर देते हैं।
इस तरह न चिरंजीलाल बचेगा, न उसका शहनाई वादन। सरकार मेलों को संस्कृति की धरोहर बताकर उसमें उन कलाकारों पर पैसा लुटाती है, जो आधुनिक संचार माध्यमों के जरिए नाम और दाम कमा चुके होते हैं।
दरअसल, ऐसे कलाकारों का संरक्षण देश का धनाढ्य वर्ग करता है, जैसा किसी समय राजा किया करते थे। पर लोक कलाकार को तो उसका गांव सुरक्षा प्रदान करता था, जो आज की परिस्थितियों में लुप्त होता नजर आ रहा है।
सामूहिकता के बिना नहीं बचेगी लोक संस्कृति
जो भी हो, लोक संस्कृति को बचाना इसलिए भी जरूरी है कि लोकसंस्कृति से अभिजात संस्कृति का निर्माण होता है। जब भारतीय सिनेमा के संगीत में ठहराव आया तो एसडी बर्मन जैसे संगीत निर्देशकों ने बंगाल के लोकगीत और लोकसंगीत की संजीवनी लाई थी।
लोक संस्कृति के इस सांस्कृतिक ग्लेशियर को बचाने के लिए जिस सामूहिकता की जरूरत है, वर्तमान समय उसके अनुकूल नहीं है। हमारा सामाजिक ढांचा चरमर्रा कर बिखर रहा है। ऐसे में किसी तरह की सामाजिकता का उभरना लगभग असंभव प्रतीत होता है।
सामूहिकता के बिना न लोक बचेगा न लोक संस्कृति। हिमाचल प्रदेश में लोक देवता इस सामूहिकता के प्रतीक हैं। इनके देव मंदिर हमारी लोक संस्कृति के रंगमंच का काम करते आए हैं। इन्हीं के आंगन में नाटियां डाली जाती थीं । वहीं बांठड़ा भी जम जाया करता था। इन्हीं देव मंदिरों में लोक संस्कृति के संरक्षण की सामर्थ्य भी है ।
देव सदन हों सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र
इन्हीं के संसाधनों का उपयोग करते हुए हम सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अपेक्षा कलात्मक सुरुचिपूर्ण एवं लोकचेतना की उन्नति के अनुकूल कार्यक्रम विकल्प के तौर पर प्रस्तुत कर सकेंगे।
मेरा संस्कृति प्रमियों से अनुरोध है कि वे इस समस्या पर विचार साझा करें, ताकि जिस सामूहिकता की हमें तलाश है, उसके पदचिन्ह पहचान सकें। देव मंदिरों और देव सदनों को सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बनाएं। यहां से लोकसंस्कृति सवंर्द्धित हो सकती है। हमें संस्कृति के संरक्षण की अपेक्षा संवर्द्धन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
( सुंदर लोहिया ने विशेष अनुरोध पर साल 2014 में यह स्तंभ लिखा था )
इस विषय से संबन्धित अन्य पोस्टें –